‘विराम’ का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखनकार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है।
इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाता है।
जैसे-
- रोको, मत जाने दो।
(भाव – पकड़ लो)
रोको मत, जाने दो।
(भाव – छोड़ दो) - खेलो, मत बैठो।
(भाव – खेलते रहो)
खेलो मत, बैठो।
(भाव शान्त रहो)
- श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिह्न 20 होते हैं।
- श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्णविराम (1) को छोड़कर अन्य विराम चिह्न अँग्रेजी भाषा से लिए गए हैं।
आधुनिक हिन्दी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं-
१. पूर्ण विराम (1) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- हमें बिजली-पानी की बचत करनी चाहिए।
हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।
२. उप विराम (:) – किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं।
जैसे- विज्ञान : वरदान या अभिशाप।,
प्रदूषण : एक समस्या।
दीपक : क्या तुम बाजार जा रहे हो?
सोनू : नहीं, अभी नहीं।
३. अर्द्धविराम (;) – जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्द्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्द्धविराम के स्थान पर अल्पविराम (,) का भी प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे- वह एक धूर्त आदमी है; ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। उसकी माँ बीमार है; इसलिए वह स्कूल नहीं गया।
४. अल्पविराम (,) – अल्पविराम का क्षेत्र व्यापक होता है। इसका प्रयोग कम ठहराव लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है-
I. जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द (और, तथा, एवं, व आदि) की गुंजाइश हो, तो उस स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- राम सुन्दर, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति थे। दीपू एक सच्चा, ईमानदार, निडर और मेहनती पुलिस ऑफिसर है।
II. ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी। वह स्वभाव का सख्त है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
III. दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- रावण, लंका का राजा, एक विद्वान था। सुभाष, जिनके विषय में तुम बात कर रहे थे, बहुत अच्छे लेखक हैं।
IV. यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द (जैसे- पर, इसलिए, जो, तो, किन्तु, परन्तु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि) प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है।
जैसे- तुम्हारा घर दूर है, इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। मैं वापस आया था, किन्तु तुम जा चुके थे।
V. किसी व्यक्ति को सम्बोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे- दीपा, एक गिलास पानी देना। राजन, तुम कल क्यों नहीं आए थे?
VI. कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है। – ‘वहाँ’ शब्द के स्थान पर
वह कब तक आयेगा, कहा नहीं जा सकता। – ‘यह’ शब्द के स्थान पर
VII. प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है।
जैसे- वैज्ञानिकों ने कहा, “पानी अमृत है, इसे बर्बाद मत करो।” जया ने कहा, “मैं कल ही घर से आई हूँ।”
VIII. हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। बस, इतनी छोटी सी बात थी। सचमुच, हम वहाँ जाएँगे।
५. प्रश्नवाचक चिन्ह (?) – प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अन्त में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- दादा जी कब आयेंगे?
वहाँ कौन था?
प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं।
कभी-कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं।
जैसे- क्या बताऊँ श्रीमान, वह कब, कहाँ जाता है, किसी को नहीं पता। राजीव ने मुझको बताया था कि वह कल कहाँ गया था।
ध्यान रहे, प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता।
शिक्षक ने प्रश्न पूछा (x)
शिक्षक ने प्रश्न किया (√)
६. विस्मयादिबोधक चिन्ह (!!) – किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे: जया! दरवाजा खोल दो। अरे! तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। आह! कितना कठिन समय है।
७. उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह- इस चिन्ह के दो रूप हैं- (i) इकहरा उद्धरण चिन्ह (ii) दोहरा उद्धरण चिन्ह
(i) इकहरा उद्धरण चिन्ह ( ” )- किसी शब्द / वाक्यांश / वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचारपत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- ‘पूस की रात’, ‘मुन्शी प्रेमचन्द’, ‘रामचरित्रमानस’, ‘दैनिक जागरण’ आदि।
(ii) दोहरा उद्धरण चिन्ह ( )- परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- सक्सेना ने कहा, “धीरे-धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत ही मिलती है।”
“उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ती तक रूको मत।”
८. योजक चिन्ह / संयोजक चिन्ह / सामासिक चिन्ह (-) इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, जिन पदों के दोनों खण्ड प्रधान हो तथा जिनमें ‘और’ लुप्त हो, सहचर शब्दों के बीच, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, कारक चिन्ह के स्थान पर, ‘सा, सी, से’ आदि से पहले, लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अन्त में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खण्ड के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- विपरीतार्थक :- लाभ-हानि, इधर-उधर, पाप-पुण्य, माता-पिता,
दोनों खण्ड प्रधानः-दाल-रोटी, हवा-पानी, लोटा-डोर
‘और’ लुप्तः- राम और लक्ष्मण = राम-लक्ष्मण,
सहचर शब्द:- काम-धाम, समझ-बूझ, हँसी-खुशी, तन-मन-धन
संयुक्त क्रियाएँ:- पढ़ना-लिखना, मारना-पीटना
शब्द दो बार प्रयुक्तः- धीरे-धीरे, राम-राम, बार-बार
कारक के स्थान परः- पद के भेद पद-भेद, रावण का वध = रावण-वध ‘सा, सी’ से पहलेः- चाँद-सा रूप, रात-सी अँधेरी, कौन-सा व्यक्ति
९. निर्देशक चिन्ह ( – ) – यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह
का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- दीपू – तुम कहाँ जा रही हो?
सीमा – मैं बाजार जा रही हूँ।
आत्मनिर्भरता-अपने ऊपर भरोसा-अपनी मेहनत का सहारा ही उन्नति का मूलमंत्र है।
नोट, जैसे-, उदाहरण-
१० . विवरण चिन्ह (:-) – किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में
विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता
है
जैसे- वनों से निम्नलिखित लाभ हैं:-
विशेषः, नोटः, जैसे:-, उदाहरण:-
११. कोष्ठक चिन्ह ‘ [ ], () ‘- वाक्य में प्रयुक्त पदविशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग होता है। चिन्हों का प्रयोग होता है।
जैसे-
सहर (सुबह) होते ही मजदूर घर से निकल पड़े।
वह अनवरत (लगातार) दौड़ता रहा।
१२. विस्मरण चिन्ह/हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह ( ^ )- जब किसी वाक्य
अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं।
जैसे- मैं पिता जी के साथ गया।
बाजार
कार्य हमें रोजाना अपना करना चाहिए।
१३. लाघव चिन्ह / संकेत चिन्ह (०) –
लघु (छोटा) से लाघव बना है। किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप (संक्षिप्त रूप) को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- उत्तर प्रदेश के लिए – डॉक्टर के लिए डॉ० उ० प्र०
१४. लोप चिन्ह (…………) –
इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गये अंश के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है।
जैसे- सीमा ने लम्बी सांस लेते हुए कहा, “मैं तुम्हारे साथ आना चाहती तो हूँ, पर सोचती हूँ कि कहीं तुम चलो ये सब छोड़ो।”
१५. दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह (SS) –
हिन्दी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- मीऽऽरा, जल्दी भागो। सोऽऽहन, मम्मी बुला रही है।
१६. पुनरूक्ति या अनुवृत्ती चिन्ह (“,”) – एक ही शब्द को बार-बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है-
| वस्तु का नाम | मात्रा |
| चीनी | 5 किलो |
| चावल | 10किलो |
| आटा | 10किलो |
१७. टीका सूचक चिन्ह ( * / + / # /1,2,3) – जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है, और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो, तो उस शब्द पर एक चिह्न लगाया जाता है, और उसी चिह्न को पैराग्राफ से अलग लगाकर वो सूचना लिखी जाती है, ऐसे चिह्न को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं।
जैसे-
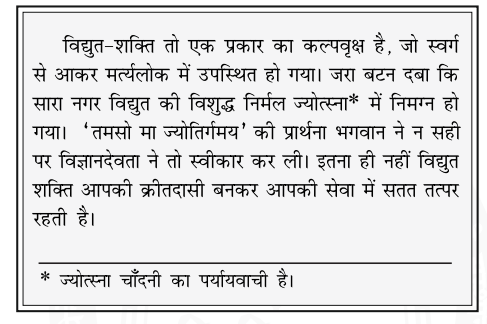
१८. रेखा चिन्ह –
जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है, उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे- जो विद्या की इच्छा रखता है, वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवनभर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है। इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है, किन्तु स्थूल रूप से मानव-जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है, फिर भी विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हँसने-हँसाने का समय है। खेल-खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है।
१९. तुल्यतासूचक चिन्ह ( = ) –
किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता-सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे- पाषाण = पत्थर, धरा = पृथ्वी
२०. अथवा चिन्ह (/)-
किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे-
गाय / घोड़ा, आकाश / पृथ्वी
२१. समाप्ति सूचक चिन्ह (—–0—–)- किसी लेख अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
